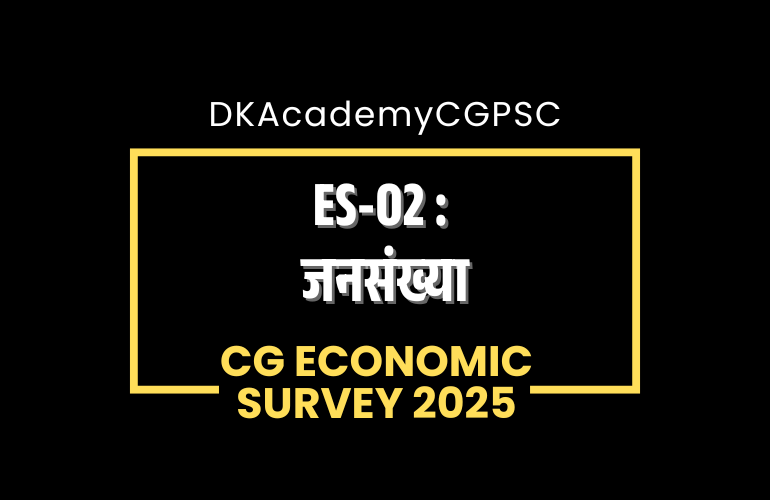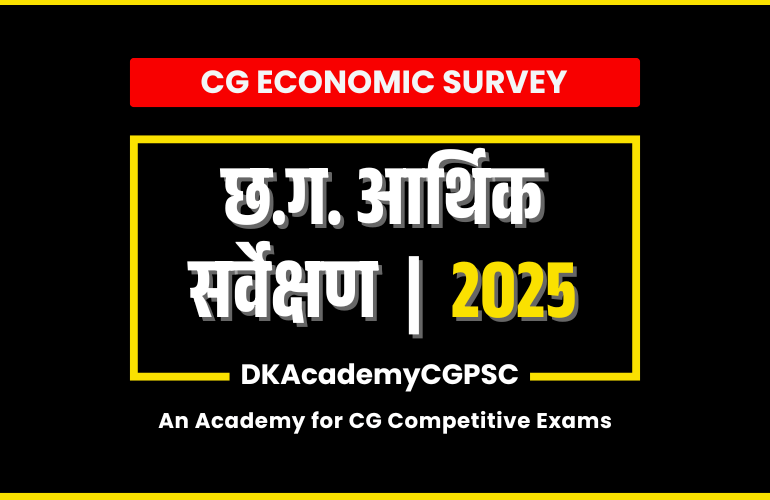Chapter 2 : Population [CG Economic Survey 2024-25]
मुख्य बिन्दु
जनसांख्यिकी आंकड़े (Demographic Data) किसी देश, राज्य या क्षेत्र की जनसंख्या से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये आंकड़े सरकार, शोधकर्ताओं, नीति-निर्माताओं और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और विकास से जुड़े निर्णयों को प्रभावित करते हैं।
1. नीति निर्माण में सहायक- जनसंख्या के आकार, संरचना और वितरण को समझकर सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, और बुनियादी ढांचे से संबंधित नीतियां बना सकती है। समाज के कमजोर वर्गों की पहचान कर उनके उत्थान के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
2. आर्थिक विकास और योजना श्रम शक्ति, बेरोजगारी दर और उत्पादकता से जुड़े आंकड़ों के आधार पर आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है। किसी क्षेत्र की जनसंख्या घनत्व और श्रमिकों की उपलब्धता को देखते हुए उद्योगों की स्थापना की जा सकती है।
3. स्वास्थ्य और जनकल्याण जन्म दर, मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और रोगों से संबंधित आंकड़े स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में मदद करते हैं। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं।
4. शिक्षा और साक्षरता- साक्षरता दर और शिक्षा स्तर के आधार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाता है। स्कूलों, कॉलेजों और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या और स्थान तय करने में सहायक ।
5. संसाधन प्रबंधन और शहरीकरण तेजी से बढ़ती जनसंख्या के आधार पर जल, बिजली, परिवहन और अन्य संसाधनों का उचित वितरण किया जाता है। शहरों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखकर स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढांचे की योजनाएं बनाई जाती हैं।
6. प्रवास और रोजगार के अवसर प्रवासन से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि लोग किस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। इन आंकड़ों के आधार पर रोजगार के अवसर बढ़ाने और शहरीकरण की समस्याओं को हल करने की दिशा में काम किया जाता है।
7. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन बढ़ती जनसंख्या के प्रभाव को देखते हुए पर्यावरणीय नीतियां बनाई जाती हैं। प्राकृतिक संसाधनों के अति-उपयोग को रोकने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आंकड़े उपयोगी होते हैं।
8 . चुनाव और राजनीतिक रणनीति- जनसंख्या के लिंग अनुपात, आयु संरचना और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियां बनाने के लिए जनसांख्यिकीय आंकड़ों का उपयोग करते हैं।
निष्कर्ष
जनसांख्यिकी आंकड़े न केवल किसी क्षेत्र की मौजूदा सामाजिक-आर्थिक स्थिति को समझने में सहायक होते हैं, बल्कि वे भविष्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं की नींव भी रखते हैं। सही आंकड़ों के आधार पर बनाई गई नीतियां समाज को अधिक समृद्ध और संतुलित बना सकती हैं।

शहरी जीवन में लोगों का बढ़ता प्रतिशत कई प्रवृत्तियों और निहितार्थों को दर्शाता है:
(1) शहरीकरण आम तौर पर, ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाकों से उच्च संभावनाओं, बुनियादी ढांचे और बेहतर रहने की स्थिति वाले शहरों में जा रहे हैं।
(2) आर्थिक विकास शहर, एक सामान्य नियम के रूप में, अक्सर अधिक नौकरियाँ, उद्योग और व्यवसाय के अवसर प्रदान करने में सक्षम होते हैं, जिससे बहुत सारे कर्मचारी और निवेशक आकर्षित होते हैं।
(3) बुनियादी ढांचा विकास यह बढ़ती शहरी आबादी के लिए बेहतर सड़कों, सार्वजनिक परिवहन, आवास और उपयोगिताओं के लिए शहरी विकास को बढ़ावा देता है।
(4) संसाधन दबाव – पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की उच्च माँग एक शहर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की सीमाओं को बढ़ाती है।
(5) जीवन शैली में बदलाव शहरीकरण संस्कृति, उपभोग के पैटर्न और सामाजिक व्यवहार को बदलती है।
(6) स्मार्ट शहर और प्रौद्योगिकी विकास सरकारों द्वारा स्मार्ट बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं और शहरी नियोजन समाधानों में निवेश शुरू करने से नई संभावनाएँ उत्पन्न होती है। os ogk
राज्य स्थापना के समय वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ में शहरी क्षेत्र (स्थानीय निकायों) की संख्या 75 थी तथा दिसम्बर 2024 तक संख्या बढ़कर 192 हो गयी है, इसी प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी जनसँख्या का प्रतिशत वर्ष 1901 से लगातार वृद्धि प्रदर्शित है तथा मार्च 2025 में छत्तीसगढ़ राज्य की शहरी जनसँख्या, कुल जनसंख्याँ का 27.26 प्रतिशत अनुमानित है। यह राज्य को सर्वांगीण विकास की ओर अग्रसर बनाती है।
तहसीलों और जिलों की संख्या में वृद्धि कुछ बदलते रुझानों और प्रशासनिक पहलुओं का संकेत भी देती है।
1. जनसंख्या में वृद्धि
जनसंख्या के आकार में वृद्धि से पहले से मौजूद तहसीलों और जिलों का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित नहीं किया जा सकता। विभाजन का एक बड़ा हिस्सा बेहतर शासन और सार्वजनिक सेवाओं के लिए क्षेत्रों और स्वायत्तता में निहित होगा।
2. प्रशासन का विकेंद्रीकरण
जिलों और तहसीलों की बढ़ती संख्या स्थानीय सरकार को लोगों के दरवाजे तक प्रशासन लाकर अधिक कुशल बनाती है। यह भूमि, करों, कानून प्रवर्तन और विकास परियोजनाओं के रिकॉर्ड को संभालने की दक्षता में सुधार करता है।
3. आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार
संसाधनों और निवेश योजना का बेहतर प्रबंधन कर क्षेत्रों में आर्थिक विकास उद्योगों, व्यवसायों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई की स्थापना करता है।
4. बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण
नए जिलों और तहसीलों के निर्माण के साथ, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कानून प्रवर्तन आदि जैसी सरकारी सेवाओं तक अधिक प्रभावी/आसान पहुँच प्रदान करना संभव है। आपदा प्रबंधन और सामाजिक कल्याण वितरण में मदद करता है।
5. क्षेत्रीय स्वायत्तता और जातीय विचार कुछ स्थानीय जातीय, सांस्कृतिक या भाषाई समुदायों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए अलग-अलग जिलों या तहसीलों के निर्माण की माँग होती है जिसके फलस्वरूप सुशासन सुनिश्चित करने और प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने में सहयोग मिलता है।

जनसंख्या घनत्व के प्रकारः
1. उच्च जनसंख्या घनत्वः जैसे कि बड़े शहरों में, जहां बहुत अधिक लोग एक छोटे क्षेत्र में रहते हैं, जैसे कि रायपुर जिले की की जनसँख्या घनत्व वर्ष 2025 के लिए सर्वाधिक 960 अनुमानित है।
2. निम्न जनसंख्या घनत्वः जैसे ग्रामीण या जंगलों में, जहां कम लोग विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, जैसे कि बीजापुर जिले की जनसँख्या घनत्व न्यूनतम 32 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वर्ष 2025 हेतु अनुमानित है। यह एक महत्वपूर्ण मापदंड है जो किसी क्षेत्र की जीवनशैली, विकास और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है।

Source:- (1)- Census 2001, Census 2011, (2) National Commission on Population, MoHFW, Gol
Remark: Data for 2001 & 2011 are actual data, while the rest are estimated data.

जनसंख्या घनत्व
1. जनसंख्या का दबावः जनसंख्या घनत्व अधिक होने पर यह दर्शाता है कि उस क्षेत्र में अधिक लोग रह रहे हैं, जिससे संसाधनों (जैसे भोजन, पानी, चिकित्सा सुविधाएं, आवास) पर अधिक दबाव पड सकता है।
2. विकास और योजनाः उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में अक्सर बेहतर बुनियादी ढांचा, सार्वजनिक सेवाएं और आवास की मांग होती
3. विकास की असमानताः यदि एक क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, तो वहां विकास की गति धीमी हो सकती है और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता कम हो सकती है।
4. प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभावः ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तेजी से होता है,
जनसंख्या घनत्व नीति निर्धारण (च्वसपबल डोपदह) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह एक क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय दबावों को समझने में मदद करता है। नीति निर्धारण के दौरान जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण करके सरकारें और अन्य संबंधित संस्थाएं प्रभावी योजनाएँ बना सकती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के विकास और उनके निवासियों की जरूरतों को पूरा करें।
जनसंख्या घनत्व नीति निर्धारण में मदद करता है।
1. संसाधनों का उचित वितरणः
संसाधन प्रबंधन के लिए यह समझाना महत्वपूर्ण है कि उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में पानी, भोजन, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवास जैसे बुनियादी संसाधनों पर अधिक दबाव होता है। जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों के आधार पर, नीति निर्माता यह निर्धारित कर सकते है कि किन क्षेत्रों में इन संसाधनों की अधिक आवश्यकता है और कहाँ इनका वितरण सही तरीके से किया जा सकता है। जल आपूर्ति, ऊर्जा आपूर्ति, और स्वच्छता सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए योजनाएँ बनाई जा सकती है जो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में अधिक दबाव वाले होंगे।
2 शहरीकरण और बुनियादी ढांचे का विकास :
उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में शहरीकरण तेजी से बढ़ता है, और ऐसे क्षेत्रों में परिवहन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, और सार्वजनिक सेवाओं की अधिक आवश्यकता होती है। नीति निर्माता जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए बुनियादी ढांचे का विकास कर सकते है ताकि इन क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।
ट्रैफिक प्रबंधन, स्मार्ट शहरों के विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जा सकती है।
3. स्वास्थ्य सेवाओं का वितरणः
उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव बढ़ता है। जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण करके यह निर्धारित किया जा सकता है कि कहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत ज्यादा है और कहाँ अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करना चाहिए।
महामारी जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए, नीति निर्माता जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों का उपयोग करके स्वास्थ्य नीतियों और टीकाकरण कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से नियोजित कर सकते हैं।
4. आवास नीति और भूमि उपयोगः
उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आवास संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे अवैध बस्तियों, सघन आवास और भूमि मूल्य वृद्धि जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जनसंख्या घनत्व के आंकड़े यह संकेत देते हैं कि कौन से क्षेत्र में आवासीय योजनाओं की जरूरत हैं और कहाँ नए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और सस्ती आवास योजनाओं की आवश्यकता है। इसके साथ ही, भूमि उपयोग नीति (संदक नेम चवसपबल) को भी बेहतर तरीके से तैयार किया जा सकता है, ताकि पर्याप्त आवास, हरित क्षेत्र, और व्यापारिक क्षेत्रों का समुचित वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
5. शिक्षा और रोजगार योजनाएँः
शिक्षा और कौशल विकास योजनाओं का उद्देश्य उस क्षेत्र की जनसंख्या की उम्र, पेशेवर जरूरतों और रोजगार के अवसरों को ध्यान में रखना होता है। जनसंख्या घनत्व से यह भी पता चलता है कि किस क्षेत्र में अधिक युवाओं की आबादी है, जो शिक्षा और रोजगार के अवसरों की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके आधार पर, स्कूलों, तकनीकी संस्थानों, और रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जरूरतों को प्राथमिकता दी जा सकती है।
6. पर्यावरणीय प्रभाव और प्रबंधनः
अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरणीय संरक्षण और सतत विकास के लिए योजनाएँ बनाई जा सकती हैं। वायु गुणवत्ता, जल संरक्षण और कचरा प्रबंधन जैसी योजनाओं के लिए जनसंख्या घनत्व महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन बना रहे।
7. कृषि नीति और ग्रामीण विकासः कम जनसंख्या घनत्व वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, जलवायु और भूमि उपयोग पर आधारित नीति निर्धारण करना आवश्यक है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर, यह पता चल सकता है कि किस क्षेत्र में कृषि सुधार, पानी प्रबंधन और ग्रामीण विकास योजनाओं की अधिक आवश्यकता है। कृषि उत्पादन को बढ़ाने और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए योजनाएँ बनाई जा सकती हैं।
8. सामाजिक सुरक्षा और जीवन स्तरः उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन योजनाओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में अक्सर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की सेवाओं की कमी होती है। नीति निर्माता इस डेटा का उपयोग करके गरीब वर्ग के लिए योजनाएँ बना सकते हैं, जैसे कि सस्ती चिकित्सा सेवाएँ, रोजगार गारंटी योजनाएँ, और सामाजिक कल्याण योजनाएँ।
जनसंख्या भिन्नता से तात्पर्य किसी समुदाय, देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, संरचना, वितरण और वृद्धि में अंतर से है। जनसंख्या भिन्नता को दर्शाने वाले प्रमुख पहलूः
1. अलग-अलग देशों, राज्यों या जिलों में जनसंख्या घनत्व और वितरण में अंतर।
2. युवा, वयस्क और वृद्ध जनसंख्या के अनुपात में अंतर।
3. किसी क्षेत्र में पुरुषों और महिलाओं की संख्या का अनुपात।
4. विभिन्न जातियों, भाषाओं, धर्मों और परंपराओं के आधार पर जनसंख्या में विविधता ।
5. अमीर और गरीब वर्ग, शिक्षित और अशिक्षित लोगों की संख्या में अंतर।
6. विभिन्न देशों या क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु दर में अंतर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर भिन्न होती है।
किशोर जनसंख्या प्रतिशत यह दर्शाता है कि किसी देश या क्षेत्र में किशोरों का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इससे संबंधित कई शैक्षिक, स्वास्थ्य, सामाजिक, और आर्थिक नीतियाँ और कार्यक्रमों की योजना बनाई जा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण संकेतक है, जिससे नीति निर्माताओं को आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझने और उनके लिए संसाधन एवं योजनाएँ बनाने में मदद मिलती है।

युवा जनसंख्या प्रतिशत यह दर्शाता है कि किसी देश या क्षेत्र की कुल जनसंख्या में युवा वर्ग का कितना हिस्सा है। यह आंकड़ा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण नीतियों को आकार देने में मदद करता है। अधिक युवा जनसंख्या वाला क्षेत्र भविष्य में अधिक कार्यबल, उपभोक्ता, और सामाजिक बदलावों का संकेत होता है, जिससे संबंधित योजनाएँ और नीतियाँ बनाई जा सकती हैं।
आयु पिरामिड से यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या युवा है, कितनी जनसंख्या वयस्क है, और कितनी जनसंख्या वृद्धावस्था में है। इससे आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा सकता है। युवा जनसंख्या के अधिक होने पर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की मांग अधिक होगी। इसका मतलब यह है कि सरकारी योजनाओं को स्कूलों, महिलाओं के स्वास्थ्य कार्यक्रम, और किशोरों के लिए सेवाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता हो सकती है। आयु पिरामिड से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी जनसंख्या कामकाजी आयु (15-64 वर्ष) में है। अगर यह आयु वर्ग बड़ा है, तो यह संकेत करता है कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ बनानी होंगी। यदि पिरामिड का ऊपरी हिस्सा (वृद्ध जनसंख्या) अधिक है, तो इसका मतलब है कि सरकार को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और पेंशन योजनाओं को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, ताकि बुजुर्गों की देखभाल की जा सके।

(Data Source- (1) Census 2001 & Census 2011 (2) National Commission on Population, MoHFW, Gol)
जीवन प्रत्याशा किसी भी देश या समाज के विकास और समृद्धि का महत्वपूर्ण मापक है। यह न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को दर्शाता है बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को भी परिलक्षित करता है। सरकारों और संगठनों को जीवन प्रत्याशा बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक होता है।
जीवन प्रत्याशा का महत्त्वः
स्वास्थ्य स्तर का संकेतकः जीवन प्रत्याशा से यह पता चलता है कि किसी देश या क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रभावी हैं। यदि जीवन प्रत्याशा अधिक है, तो इसका अर्थ है कि वहाँ की चिकित्सा सुविधाएँ अच्छी हैं और बीमारियों की रोकथाम प्रभावी है।
आर्थिक विकास का मापकः
अधिक जीवन प्रत्याशा वाले देशों में आमतौर पर उच्च जीवन स्तर और बेहतर आर्थिक अवसर होते हैं। विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा अधिक होती है क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य सेवाएँ, पोषण और जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है।
जनसंख्या वृद्धि और संरचना पर प्रभावः
जीवन प्रत्याशा बढ़ने से बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है, जिससे पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और देखभाल प्रणालियों की आवश्यकता बढ़ती है। कम जीवन प्रत्याशा वाले देशों में युवा आबादी अधिक होती है, जिससे शिक्षा और रोजगार की अधिक आवश्यकता होती है।
सरकारी नीतियों और योजनाओं पर प्रभावः
जीवन प्रत्याशा को ध्यान में रखते हुए सरकारें स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था देखभाल से संबंधित योजनाएँ बनाती हैं। यदि जीवन प्रत्याशा कम होती है, तो इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता में सुधार की आवश्यकता है।

मध्य आयु (Median Age) वह आयु होती है, जो किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या को दो समान भागों में विभाजित करती है अर्थात, आधी जनसंख्या इस आयु से कम होती है और आधी जनसंख्या इस आयु से अधिक होती है।
मध्य आयु का महत्वः
जनसंख्या संरचना को दर्शाता है
1. यदि मध्य आयु कम है, तो जनसंख्या युवा है और जन्म दर अधिक हो सकती है।
2. यदि मध्य आयु अधिक है, तो समाज में बुजुर्गों की संख्या अधिक होती है, जिससे वृद्धजन देखभाल और पेंशन योजनाओं की मांग बढ़ती है।
आर्थिक विकास का संकेतक
1. कम मध्य आयु वाले देशों में श्रम शक्ति अधिक होती है, जिससे आर्थिक विकास की संभावनाएँ अधिक होती हैं।
2. अधिक मध्य आयु वाले देशों को वृद्ध जनसंख्या की देखभाल के लिए अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है।
स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा से संबंध
1. अधिक मध्य आयु वाले देशों में आमतौर पर स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होती है और जीवन प्रत्याशा अधिक होती है।
2. कम मध्य आयु वाले देशों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता हो सकती है।
उपरोक्त ग्राफ से निःसंदेह स्पष्ट है कि भारत वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में श्रम शक्ति का प्रतिशत अधिक है जिससे आर्थिक विकास की संभावनाए तुअल्नाताम्क रूप से अपार हैं, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन प्रत्याशा भारत वर्ष से कम है अर्थात राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की आवश्यकता हो सकती है।

CBR (Crude Birth Rate)- जन्म दर को दर्शाता है।
CDR (Crude Death Rate) मृत्यु दर को दर्शाता है।
IMR (Infant Mortality Rate) – शिशु मृत्यु दर को दर्शाता है।
TFR (Total Fertility Rate) कुल प्रजनन दर) किसी क्षेत्र की महिलाओं द्वारा जीवनकाल में औसतन
जन्म दिए गए बच्चों की संख्या को दर्शाता है।
ये चारों संकेतक किसी देश या क्षेत्र की स्वास्थ्य प्रणाली और सामाजिक-आर्थिक विकास को मापने में मदद करते हैं।
उच्च CBR वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक होती है।
उच्च CDR किसी क्षेत्र में खराब स्वास्थ्य सेवाओं या जीवन स्तर को दर्शा सकता है।
उच्च IMR का अर्थ है कि स्वास्थ्य सेवाएँ और शिशु देखभाल की स्थिति खराब है।
यदि TFR 2.1 है, तो इसे जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर (Replacement Level Fertility) कहा जाता है, जहाँ अगली पीढ़ी जनसंख्या को बनाए रखने के लिए पर्याप्त होती है। यदि किसी देश में TFR बहुत अधिक (जैसे 4 या 5) है, तो वहाँ जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी यदि TFR 2.1 से कम है, तो जनसंख्या धीरे-धीरे घट सकती है, जिससे भविष्य में बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी और श्रम शक्ति में कमी आएगी। जनसंख्या को बनाए रखने के लिए TFR का 2.1 होना आवश्यक माना जाता है।



See also
References
Take an online test on the CG Economic Survey and CG Budget from the DKAcademyCGPSC App.
***